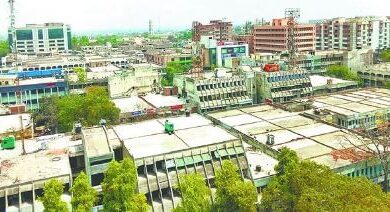आरबीएस इंजीनियरिंग के छात्रों ने कचरे से स्वास्थ्य का अनमोल खजाना खोजा।

फल और सब्जी के छिलके जो हम कचरे में फेंकते हैं, वास्तव में पोषण के धरोहर हैं। हरे मटर के छिलको में विटामिन बी1, बी2, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। इसी तरह, आम के गुठली में भी कई पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं।
राजा बालवंत सिंह इंजीनियरिंग तकनीकी परिसर में, खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग ने ग्रीन मटर के छिलके और आम की गुठली को संसाधित करके बिस्कुट और कस्टर्ड पाउडर बनाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि हम इन अनुपयुक्त चीजों को कचरे में फेंकने के बजाय उनका सही उपयोग कर सकें और पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बना सकें।
खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के शिक्षक अमित प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में छात्र निखिल चौहान, श्रुति त्रिपाठी, वरशा चाहर, यश राठौर और वतन कुमार ने वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए मटर का उपचार किया। मटर के छिलके को उचित तापमान पर सुखाकर पाउडर बनाया गया। इस पाउडर को विभिन्न अनुपात में आटे के साथ मिलाकर बिस्कुट तैयार किए गए, और सर्वश्रेष्ठ बिस्कुट का चयन तकनीकी विश्लेषण और संवेदनात्मक परीक्षण के आधार पर किया गया। परीक्षण के अनुसार, मटर के छिलके से बने बिस्कुट लगभग 90 दिनों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं।
विभाग के प्रमुख प्रो. अपूर्वा विहारी लाल ने बताया कि लगभग 60 प्रतिशत मटर की फली अनाज के रूप में और 40 प्रतिशत पील के रूप में बेरोजगार रहती है। उन्होंने कहा कि हम इस अनुपात को कचरे में डालते हैं, जबकि इसमें प्रोटीन और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इनका उपयोग करके हम न केवल अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं।
आम की गुठली पर भी डॉ. आशीष खरे के नेतृत्व में शोध किया गया। उन्होंने बताया कि आम की गुठली को पहले पके हुए आम से निकाला गया था। फिर गुठली के कठोर आवरण को हटा दिया गया और अंदर के बीज को छोटे टुकड़ों में काटकर वैज्ञानिक विधियों से पाउडर बनाया गया। इस पाउडर में लगभग 80 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, 9 प्रतिशत प्रोटीन, तथा आवश्यक खनिज और फाइबर भी हैं। इसमें जैव-सक्रिय यौगिक भी पाए जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं।
बेल के फल के बाहरी हिस्से पर भी अनुसंधान किया गया। अध्ययन के दौरान, बेल के स्किन को सुखाकर पाउडर बनाया गया और इसे खाद्य उद्योग में उपयोग करने योग्य सामग्री में परिवर्तित किया गया। बेल के छिलके में सेलूलोज पाया जाता है, जिसका उपयोग स्थिरीकरण और पैकेजिंग सामग्री बनाने में किया गया।
आरबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक प्रो. ब्राजेश कुमार ने कहा कि खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के शिक्षक और छात्र लगातार नए शोध कर रहे हैं और नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार का शोध न केवल मानव जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी सुधारने में मदद करता है।
स्वास्थ्य के लिए उद्देश्य केवल इन छिलकों और गुठलियों का उपयोग करना नहीं है, बल्कि ये सभी प्रयास हमें यह समझाने का काम कर रहे हैं कि कचरा केवल कचरा नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान संसाधन भी है। इन अनुसंधानों का उद्देश्य यही है कि हम अपनी परंपराओं को प्रगति की ओर ले जाएं और इन फालतू चीजों को नई जिंदगी दें।
यह सभी प्रोजेक्ट्स हमें यह बताता है कि प्रकृति की हमें जो चीजें मिलती हैं, वे कई बार हमसे कहीं अधिक बहुमूल्य होती हैं। हमें केवल उन्हें समझने की जरूरत है और सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है।
यह प्रयास न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। इन अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान को हमें अपनाना चाहिए और इस पर अपनी अगली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके माध्यम से, हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं।
इस तरह के अनुसंधानों का महत्व न केवल शैक्षणिक है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने चारों ओर की चीजों को समझ कर उनका उपयोग कर सकते हैं।
इसलिए, अगले बार जब आप किसी फल या सब्जी का छिलका या गुठली फेंकने जा रहे हों, तो थोड़ा सोचिए। हो सकता है कि वह आपके स्वास्थ्य के लिए एक अनमोल स्रोत हो।
समाज की भलाई और पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग देने के लिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी वस्तुओं का सही उपयोग करें जो केवल कचरा समझी जाती हैं। ये अनुसंधान और नवाचार हमें यही सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में छोटी-छोटी चीजों का महत्व समझकर अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण बना सकते हैं।
इसी प्रकार के और अन्वेषण और अनुसंधान करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकें और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग रोक सकें। ध्यान रहे, कि प्रकृति हमेशा हमारे पास है, हमें बस इसे समझने और सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है।
इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हम भविष्य के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं जो न केवल हमें बल्कि हमारे ग्रह को भी बचाए।