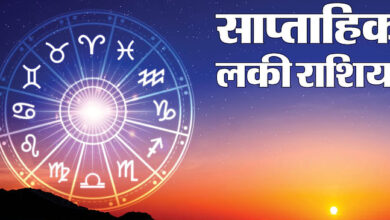तुलसी को बख्शिए: जातिवादी, दलित और स्त्री विरोधी बताकर चौतरफा हमला

उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट तब आया, जब पत्नी रत्नावली ने तुलसी को दुत्कार, अपनी देहयष्टि से ध्यान हटा भगवान में ध्यान लगाने का फरमान सुना दिया।
बाबा तुलसीदास एक बार फिर संकट में हैं। उनपर जातिवादी, दलित और स्त्री विरोधी बताते हुए चौतरफा हमला हो रहा है। उनके रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता पाबंदी की मांग की जा रही है। इस दफा तुलसी पर हमला ‘कुपढ़ों’ ने बोला है। ऐसा संकट तुलसी पर पहली बार नहीं आया है। तुलसीदास जन्मे बांदा में और मरे बनारस में। पहला संकट उनके जन्म लेते ही आया, जब एक बुरे नक्षत्र में जन्म लेने मात्र से अपशकुन मान उनके माता-पिता ने उन्हें त्याग दिया। सेविका चुनिया ने ही उन्हें पाला पोसा। पर पांच साल की उम्र में धर्ममाता चुनिया भी चल बसी। अब रामबोला दूबे पूरी तरह अनाथ थे। तुलसी बनने की प्रक्रिया में वह दर-दर ठोकर खाने लगे।
उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट तब आया, जब पत्नी रत्नावली ने तुलसी को दुत्कार, अपनी देहयष्टि से ध्यान हटा भगवान में ध्यान लगाने का फरमान सुना दिया। इस आघात से बिखरे तुलसी हनुमान की शरण में गए और संवत 1631 में हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया, बनारस में संकटमोचन मंदिर की स्थापना करने के बाद। उन्होंने लोक के बीच रामचरित को ले जाने के लिए अपना यह महाकाव्य ‘अवधी’ में लिखना शुरू किया। अब वह काशी के पंडितों के निशाने पर आ गए, क्योंकि भगवत गाथा देवभाषा यानी ‘संस्कृत’ में ही लिखी जानी चाहिए। वह गंवारों की बोली में कैसे लिखी जा सकती है! सो तुलसी जितना लिखते थे, फौरन उनका लिखा बनारस के संस्कृतनिष्ठ पंडित गंगा में फेंक देते थे। उन्हें मारते-पीटते और अपमानित अलग करते थे। इसीलिए तुलसी ने अस्सी मुहल्ले के पास के इलाके को ‘भयदायिनी’ कहा, जो आज ‘भदैनी’ नाम से जाना जाता है।
रामचरितमानस की गिनती विश्व की महान कृतियों में होती है। गांधी जी ने मानस को ‘भक्ति साहित्य की श्रेष्ठ कृति’ कहा। अफसोस कि मानस को लिखे जाने के कोई पांच सौ बरस बाद उसे 21वीं सदी के विमर्शों और सामाजिक आधारों की कसौटी पर कसा जा रहा है। रामचरितमानस पर अकादमिक बहस हो सकती है, पर किसी महाकाव्य से सिर्फ दो पंक्तियां उठा समूचे ग्रंथ के प्रति दुर्भावना फैलाना अक्षम्य अपराध है। तुलसी को समझने के लिए हमें मानस से लेकर विनय पत्रिका तक की पूरी यात्रा करनी पड़ेगी। तुलसी पूरी संवेदना के साथ अपने समाज के यथार्थ से टकराते ही नहीं, रामराज्य का विकल्प भी देते हैं। हर साहित्यकार के पास अपना एक ‘यूटोपियन’ समाज भी होता है। तुलसी के पास भी था। मार्क्स के पास भी था। तुलसी उसे रामराज्य कहते हैं। गोर्की कहते थे, ‘सबसे सुंदर बात है अच्छी बातों की कल्पना करना। यह कल्पना किसी रचनाकार की उदात्तता का प्रमाण होती है।’ तुलसी किसी भी युग के रचनाकारों से इसलिए भिन्न हैं कि वह सबसे कठिन समय में ‘आदर्श युग’ की कल्पना करते हैं। रामराज्य की कल्पना से वह ऐसे युग का सपना रोपते हैं, जहां- बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई॥ सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥ अगर वह अपने युग सत्य को छोड़ते, तो उनकी लेखकीय ईमानदारी का क्या होता?
ताजा विवाद में गड़बड़ दोनों तरफ है। न उन्हें परंपरा का ज्ञान है, न इतिहास का। तुलसी का रचना संसार उन्हें भगवान मानने और कुछ न मानने वालों के बीच में फंस गया है। एक तरफ वे मूढ़ हैं, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि जब तुलसीदास लिख रहे थे, उस वक्त न मंडल कमीशन आया था, न सिमोन द बुआ का नारी विमर्श आया था। दूसरी तरफ वे लोग हैं, जो मानस को सिर्फ धार्मिक और पूजा भाव से पढ़ते हैं। रामचरितमानस वैसा ही काव्य है, जैसा उनके समकालीन जायसी का पद्मावत, केशव की रामचंद्रिका, नाभादास का भक्तमाल, सूर का सूरसागर या कबीर की रमैनी, सबद और साखी। सब अपने-अपने समय के समाज की आवाज को अभिव्यक्त कर रहे थे। रामचरितमानस बहुचरित्र महाकाव्य है, जो विराट कथानक और धीरोदात्त नायकत्व के मूल्यों पर केंद्रित है। जिसका नायक संघर्षों से तप कर आता है। तुलसी के राम पराजित, दुखी, आदर्शों और संकल्पों के सामने जीवन का सब कुछ गंवा देने वाले नायक हैं। सामान्य भारतीय का संघर्ष यही है, इसलिए वह राम से सीधा जुड़ जाता है। डॉ. लोहिया कहते हैं,’नारी की पीड़ा को तुलसी जिस ढंग से व्यक्त करते हैं, उसकी मिसाल भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी साहित्य में नहीं है।’ तुलसी जातिवादी नहीं हो सकते, क्योंकि वह भक्त हैं। भक्ति सर्वहारा का आंदोलन है। वहां जाति, कुल, गोत्र का विचार नहीं, केवल साधना कसौटी है। अगर हम जाति और समाज विभाजन की युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में रामचरितमानस को पढ़ें, तो समझ आएगा कि तुलसी ने जानबूझकर समाज के वे सारे चरित्र चुने, जो मुख्यधारा में नहीं थे।
मसलन निषाद, वनवासी, शबरी, वानर, पक्षियों में त्याज्य कौआ यानी परमज्ञानी ‘काकभुशुंडि’। अगर ये सब न भी होते, तो राम को रावण से युद्ध करा विजेता दिखा नायक बनाया जा सकता था। पर तुलसी राम की जीत में देवत्व स्थापित नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने जातियों का सच लिखा। बल्कि तुलसी तो जाति की जकड़न को तोड़ रहे थे। उन्हें लिखना पड़ा, मेरे ब्याह न बखेरी जाति पाति न तहत हौं। जब उन पर लोग जाति तोड़ने का आरोप लगाने लगे, तो खीज में वह अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रूचे सौ कहै कछु कोऊ। मांगि के खैबो, मसीत को सोइबो, लैबो को एकु न दैबो को दोऊ। जाति के पचड़े से वह इस कदर ऊबे थे कि मांग कर खाने और मस्जिद में सोने को भी तैयार थे। जातिवादी ब्राह्मणों ने उन्हें षड्यंत्रकारी, दगाबाज और अनेक कुसाजों को रचने वाला बताया। तुलसी ने भी पथभ्रष्ट ब्राह्मणों की निंदा की-विप्र निरच्छर लोलुप कामी।
निराचार सठ बृषली स्वामी।। इसके बाद भी तुलसी को कैसे ‘ब्राह्मणवादी’ कह सकते हैं? याद कीजिए, चित्रकूट की रात्रिसभा। भरत ग्लानि से भरे हैं। अयोध्या का बहुमत राम को वापस लाने के पक्ष में था। राम नहीं लौटते। राम ने जनमत की उपेक्षा क्यों की? यह राम की राजनीति का स्वर्णिम पक्ष है। राम पहले भरत को दोषमुक्त करते हैं। फिर कैकेयी की ग्लानि समाप्त करते हैं। फिर वह भरत के जरिये अयोध्या वासियों से कहते हैं कि राजा से वही कराएं, जो उचित हो। यह राजनीति की राम परिभाषा है। राजनीति को कीर्तिमयी- सद्भावमयी होना चाहिए। तुलसी का पूरा साहित्य इसी समाज और राजनीति की संकल्पना है। काश, हम अपनी दृष्टि व्यापक कर पाते, तो रामचरितमानस में जातिवाद नहीं, त्याग और लोकतंत्र देख रहे होते!